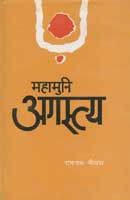|
सांस्कृतिक >> ठिठुरती धूप ठिठुरती धूपरामनाथ नीखरा
|
101 पाठक हैं |
||||||
दुःख दैन्य,शोषण एवं उत्पीड़नजन्य शीत से काँपती की ठिठुरती धूप....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
उपोद्धात
धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति एवं राजनीति इन सबका प्रधान लक्ष्य
है—मुनष्य को शिक्षित, संस्कारित कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों
में व्याप्त वैषम्य को न्यूनातिन्यून करते हुए प्रचलित पथ, मत, वाद एवं
अवधारणाओं के मध्य समन्वय व सामंजस्य की स्थापना का प्रयास करना तथा
व्यापक स्तर पर समस्त मानव समाज के कल्याण की योजना करना। परंतु, क्या
इनमें से किसी को भी स्वीकृत लक्ष्यों की संप्राप्ति में अभीष्ट सफलता
प्राप्त हुई है या प्राप्त हो रही है ?
नहीं। क्यों ? क्योंकि जिन विशिष्ट उद्देश्यों के पूर्त्यर्थ इन संस्थाओं का सृजन किया जाता है या किया गया है, प्रयोगकर्ता उन्हें विस्मृत भर नहीं करते, वरंच उन्हें इतना विकृत कर देते हैं कि वे समष्टि के स्थान पर व्यष्टि के हितसाधन का अभिकरण बनकर रह जाते हैं। ऐसा संस्था-विशेष के साथ ही हुआ हो या होता हो, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, सभी के साथ ऐसा ही होता है या हो सकता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि आज धर्म बाह्माडंबर, दर्शन पूर्वग्रहों की पुष्टि का साधन, अर्थ निर्बल व निर्धन लोगों के शोषण का अभिकरण, शिक्षा तथ्यों व सूचनाओं का संकलन, संस्कृति पृथक पहचान के बहाने पृथकत्व की संपुष्टि का माध्यम तथा राजनीति विरोधियों के दमन, पीड़न तथा सत्ता के अनियंत्रित उपयोग का अस्त्र बनकर रह गए हैं। ऐसी अवस्था में क्या यह आशा की जा सकती है कि उपरिनिर्दिष्ट संस्थाएँ वैषम्य को न्यूनातिन्यून कर समन्वय व सामंजस्य की स्थापना का प्रयास करेंगी ? अधिसंख्य मानव के कल्याणार्थ अपने आप को नियोजित करेंगी ? कम-से-कम आज के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण में तो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता।
तो क्या धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति व राजनीति से समग्रतः मुक्ति प्राप्ति में ही हम सब की निष्कृति है ? नहीं, क्योंकि प्रस्तुत परिवेश में भी समस्त अपदाओं से मुक्ति पाने की एक मात्र आशा इन्हीं संस्थाओं के सदुपयोग पर निर्भर करती है। यह भी कहा जा सकता है कि स्थिति के भयावह होने पर भी आज इनकी सह्यता केवल इसलिए बनी हुई है कि ये संस्थाएँ किसी-न-किसी रूप में जाने-अनजाने आज भी मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं और किसी-न-किसी परिणाम में मानव का हित भी कर रही हैं। अतः इनकी संपूर्णतः उपेक्षा मानव-कल्याण की दृष्टि से अनुचित ही नहीं, हानिकारक भी है।
फिर एक बात और विचारणीय है, और वह यह कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति गेहूँ में कचरा होने पर उसे हटाने का उपक्रम करता है, कचरे से घबड़ाकर समस्त गेहूँ को ही सड़क पर नहीं फेंकता। ठीक इसी प्रकार इन संस्थाओं में जो विकृतियाँ हैं, उन्हें ही दूर करना होगा। इन संस्थाओं को ही समाप्त करने की न तो कोई उपयोगिता है, और न सार्थकता ही।
अब प्रश्न यह आता है कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाए ? किस संस्था को प्राथमिकता दी जाए ? इसके उत्तर में विद्वज्जनों का मत है कि हमें सर्वप्रथम राजनीति को परिष्कृत-परिमार्जित करना होगा; क्योंकि धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा एवं संस्कृति में जो विकृतियाँ हैं, उनकी पृष्ठभूमि में राजनीति और मात्र राजनीति ही रहती है। रहे भी क्यों नहीं ? सत्ता समस्त लौकिक सुखों की जननी है, अतः सत्ता की प्राप्ति तथा उसके स्वच्छंद भोग की लालसा ने आज सबको राजनीति-सापेक्ष बना दिया है। सचाई तो यह है कि आज हमारे समस्त क्रियाकलाप की धुरी राजनीति हो गई है।
धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा एवं संस्कृति—इन सबकी पृथक सत्ता तो यह है, परंतु आज इनका घूर्णन राजनीति की धुरी पर ही हो रहा है। यही नहीं, आज इन सबको गति व दिशा राजनीति से ही प्राप्त होती है। ठीक भी है, ‘राजा कालस्य कारणम्’ के सिद्धांतानुसार सब प्रकार की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राज्य-शासन तथा उसकी रीति-नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
और राजनीति ? राजनीति का स्वरूप चाहे एकतंत्रात्मक हो या जनतंत्रात्मक, चाहे अधिनायकवादी हो अथवा समाजवादी या साम्यवादी, सामान्यतः उसका संचालन-सूत्र कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में ही रहता है। अतः कतिपय अपवादों को छोड़कर उसका उपयोग प्रायः कुछ व्यक्तियों अथवा व्यक्ति-समूहों के कल्याणार्थ ही होता है और हो भी रहा है। अतएव जो लोग प्रस्तुत विकृति राजनीति के माध्यम से जनसामान्य की सुख-समृद्धि तथा शांति की आशा कर रहे हैं, कविवर प्रसाद के शब्दों में उन्हें भी अपरोक्ष सत्ता से यही प्रार्थना करनी चाहिएः
नहीं। क्यों ? क्योंकि जिन विशिष्ट उद्देश्यों के पूर्त्यर्थ इन संस्थाओं का सृजन किया जाता है या किया गया है, प्रयोगकर्ता उन्हें विस्मृत भर नहीं करते, वरंच उन्हें इतना विकृत कर देते हैं कि वे समष्टि के स्थान पर व्यष्टि के हितसाधन का अभिकरण बनकर रह जाते हैं। ऐसा संस्था-विशेष के साथ ही हुआ हो या होता हो, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, सभी के साथ ऐसा ही होता है या हो सकता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि आज धर्म बाह्माडंबर, दर्शन पूर्वग्रहों की पुष्टि का साधन, अर्थ निर्बल व निर्धन लोगों के शोषण का अभिकरण, शिक्षा तथ्यों व सूचनाओं का संकलन, संस्कृति पृथक पहचान के बहाने पृथकत्व की संपुष्टि का माध्यम तथा राजनीति विरोधियों के दमन, पीड़न तथा सत्ता के अनियंत्रित उपयोग का अस्त्र बनकर रह गए हैं। ऐसी अवस्था में क्या यह आशा की जा सकती है कि उपरिनिर्दिष्ट संस्थाएँ वैषम्य को न्यूनातिन्यून कर समन्वय व सामंजस्य की स्थापना का प्रयास करेंगी ? अधिसंख्य मानव के कल्याणार्थ अपने आप को नियोजित करेंगी ? कम-से-कम आज के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण में तो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता।
तो क्या धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति व राजनीति से समग्रतः मुक्ति प्राप्ति में ही हम सब की निष्कृति है ? नहीं, क्योंकि प्रस्तुत परिवेश में भी समस्त अपदाओं से मुक्ति पाने की एक मात्र आशा इन्हीं संस्थाओं के सदुपयोग पर निर्भर करती है। यह भी कहा जा सकता है कि स्थिति के भयावह होने पर भी आज इनकी सह्यता केवल इसलिए बनी हुई है कि ये संस्थाएँ किसी-न-किसी रूप में जाने-अनजाने आज भी मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं और किसी-न-किसी परिणाम में मानव का हित भी कर रही हैं। अतः इनकी संपूर्णतः उपेक्षा मानव-कल्याण की दृष्टि से अनुचित ही नहीं, हानिकारक भी है।
फिर एक बात और विचारणीय है, और वह यह कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति गेहूँ में कचरा होने पर उसे हटाने का उपक्रम करता है, कचरे से घबड़ाकर समस्त गेहूँ को ही सड़क पर नहीं फेंकता। ठीक इसी प्रकार इन संस्थाओं में जो विकृतियाँ हैं, उन्हें ही दूर करना होगा। इन संस्थाओं को ही समाप्त करने की न तो कोई उपयोगिता है, और न सार्थकता ही।
अब प्रश्न यह आता है कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया जाए ? किस संस्था को प्राथमिकता दी जाए ? इसके उत्तर में विद्वज्जनों का मत है कि हमें सर्वप्रथम राजनीति को परिष्कृत-परिमार्जित करना होगा; क्योंकि धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा एवं संस्कृति में जो विकृतियाँ हैं, उनकी पृष्ठभूमि में राजनीति और मात्र राजनीति ही रहती है। रहे भी क्यों नहीं ? सत्ता समस्त लौकिक सुखों की जननी है, अतः सत्ता की प्राप्ति तथा उसके स्वच्छंद भोग की लालसा ने आज सबको राजनीति-सापेक्ष बना दिया है। सचाई तो यह है कि आज हमारे समस्त क्रियाकलाप की धुरी राजनीति हो गई है।
धर्म, दर्शन, अर्थ, शिक्षा एवं संस्कृति—इन सबकी पृथक सत्ता तो यह है, परंतु आज इनका घूर्णन राजनीति की धुरी पर ही हो रहा है। यही नहीं, आज इन सबको गति व दिशा राजनीति से ही प्राप्त होती है। ठीक भी है, ‘राजा कालस्य कारणम्’ के सिद्धांतानुसार सब प्रकार की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राज्य-शासन तथा उसकी रीति-नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
और राजनीति ? राजनीति का स्वरूप चाहे एकतंत्रात्मक हो या जनतंत्रात्मक, चाहे अधिनायकवादी हो अथवा समाजवादी या साम्यवादी, सामान्यतः उसका संचालन-सूत्र कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में ही रहता है। अतः कतिपय अपवादों को छोड़कर उसका उपयोग प्रायः कुछ व्यक्तियों अथवा व्यक्ति-समूहों के कल्याणार्थ ही होता है और हो भी रहा है। अतएव जो लोग प्रस्तुत विकृति राजनीति के माध्यम से जनसामान्य की सुख-समृद्धि तथा शांति की आशा कर रहे हैं, कविवर प्रसाद के शब्दों में उन्हें भी अपरोक्ष सत्ता से यही प्रार्थना करनी चाहिएः
चिरदग्ध दुखी यह वसुधा, आलोक माँगती तब भी।
तुम तुहिन बरस दो कण-कण, यह पगली सोए अब भी।।
तुम तुहिन बरस दो कण-कण, यह पगली सोए अब भी।।
संभव है, कुछ को यह प्रस्थापना सर्वथा भ्रांत अथवा अतिरंजित प्रतीत हो;
परंतु गंभीरतापूर्वक विचार करें तो हम देखेंगे कि चाहे धर्मांतरण की बात
हो, चाहे धार्मिक पुनरूत्थान की; चाहे सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का
आग्रह हो, अथवा सांस्कृतिक अभ्युत्थान का; चाहे समस्त उत्पादन-केंद्रों के
राष्टीयकरण का प्रश्न हो अथवा उन्मुक्त बाजार-व्यवस्था का सवाल; सबके मूल
में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने की भावना ही कार्य कर रही है। सब
नवीन परिवेश में प्रच्छन्न उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए
प्रयत्नशील प्रतीत होते हैं।
यह भी कहा जा सकता है कि आज राजनीति का अपराधिकरण तथा अपराधियों के राजनीतिकरण की जिस भयावह समस्या से समाज जूझ रहा है, वह भी मानव की अपरिमित अर्थ-लिप्सा तथा सत्ता-लोलुपता का परिणाम है, उसके अपने आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना के दुष्प्रयत्नों का प्रतिफल है। परंतु, निराश होकर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। यह सच है कि सामाजिक क्रांति राजनीतिज्ञों के माध्यम से नहीं, समाज-सुधारकों के माध्यम से ही होती है, फिर भी भ्रष्ट व विकृत राजनीति की भी पूर्णरूपेण उपेक्षा नहीं की जा सकती। अस्तु, आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता राजनीति के परिष्करण, परिमार्जन तथा उसे वास्तविक अर्थ में जनोन्मुखी बनाने की है, और यह तभी संभव है जब राजनीतिज्ञों व जनसामान्य की दूषित प्रवृत्तियों, उन सबकी गतिविधियों और उनके परिणामस्वरूप, समाज व शासन में उद्भूत विकृतियों तथा तज्जन्य दुष्परिणामों का ह्रदयग्राही व प्रभावी चित्रण किया जाए, और...और लेखकीय तटस्थता तथा निष्पक्षता को एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओझल न किया जाए।
क्यों ? क्योंकि यह सुनिश्चित है कि दुःख, दैन्य, शोषण एवं उत्पीड़नजन्य शीत से काँपती हुई मानवता को ठिठुरती धूप जैसी शिक्षा, संस्कृति व राजनीति कभी उष्णता प्रदान नहीं कर सकती। यह सब तभी, और मात्र तभी संभव है, जब वे स्वतः स्वस्थ हों, उनके रक्त में प्राणों की ऊष्मा हो। उन्हें स्वस्थ तथा सप्राण चित्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका चित्रण स्वस्थ चित्त से पूर्णतः तटस्थ तथा निष्पक्ष होकर किया जाए।
प्रस्तुत उपन्यास ‘ठिठुरती धूप’ में यही प्रयास किया गया है। अपने इस प्रयास में कथाकार को कितनी और क्या सफलता प्राप्त हुई है; उसका कथ्य, शिल्प तथा संप्रेष्य कितना सहज, सरस व प्रभविष्णु बन पड़ा है; यह सब तो पाठकों के विचार का विषय है। अतः उसके संबंध में यहाँ कुछ लिखना न तो उचित होगा और न न्यायसंगत ही, परंतु यहाँ यह लिखना अनुचित व असंगत न होगा कि इस उपन्यास का सृजन करते समय लेखकीय तटस्थ तथा निष्पक्षता बनाए रखने का भरसक प्रयास किया गया है। केवल संवाद लेखन के स्तर पर ही नहीं, प्रत्युत घटना-संयोजन, चरित्र-चित्रण तथा आत्मचिंतन के स्तर पर भी इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का प्रयास किया गया है।
यह भी निवेदन है कि उपन्यास के कथानक में वर्णित स्थान, पात्र, दल, संगठन, घटनाक्रम सब काल्पनिक हैं। किसी को लांछित करने के अभिप्राय से कुछ भी नहीं लिखा गया है। बस, प्रसंगवश देश में हुए राजनीतिक परिवर्तन एवं तत्कालीन केंद्र सरकार एवं कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख है, किंतु संबंधित विवरण कल्पना के नहीं, निकट अतीत के प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित हैं।
‘रिसता घाव’ उपन्यास के लेखन, प्रकाशन एवं विमोचन के पश्चात इस नवीन उपन्यास के लेखन, मुद्रण व प्रकाशन के प्रति मेरे पुत्रों—देवेंद्र, राजेंद्र, शैलेंद्र व सुधींद्र—की ही नहीं, मित्रों व शुभचिंतकों की जो उत्सुकता व आतुरता रही, उसके कारण इस उपन्यास के सृजन में तो कोई शैथिल्य एवं प्रमाद नहीं आया; परंतु कारणवश इस उपन्यास का प्रकाशन अवश्य विलंबित होता रहा।
अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस उपन्यास के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया कुछ भी क्यों न हो, परंतु इसे पढ़कर उन्होंने अपना श्रम व बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं किया, ऐसी अनुभूति उन्हें अवश्य होगी। इसी विश्वास के साथ मैं इस उपन्यास को सहर्ष सुधीजनों के करकमलों में सौंप रहा हूँ।
यह भी कहा जा सकता है कि आज राजनीति का अपराधिकरण तथा अपराधियों के राजनीतिकरण की जिस भयावह समस्या से समाज जूझ रहा है, वह भी मानव की अपरिमित अर्थ-लिप्सा तथा सत्ता-लोलुपता का परिणाम है, उसके अपने आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व की स्थापना के दुष्प्रयत्नों का प्रतिफल है। परंतु, निराश होकर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। यह सच है कि सामाजिक क्रांति राजनीतिज्ञों के माध्यम से नहीं, समाज-सुधारकों के माध्यम से ही होती है, फिर भी भ्रष्ट व विकृत राजनीति की भी पूर्णरूपेण उपेक्षा नहीं की जा सकती। अस्तु, आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता राजनीति के परिष्करण, परिमार्जन तथा उसे वास्तविक अर्थ में जनोन्मुखी बनाने की है, और यह तभी संभव है जब राजनीतिज्ञों व जनसामान्य की दूषित प्रवृत्तियों, उन सबकी गतिविधियों और उनके परिणामस्वरूप, समाज व शासन में उद्भूत विकृतियों तथा तज्जन्य दुष्परिणामों का ह्रदयग्राही व प्रभावी चित्रण किया जाए, और...और लेखकीय तटस्थता तथा निष्पक्षता को एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओझल न किया जाए।
क्यों ? क्योंकि यह सुनिश्चित है कि दुःख, दैन्य, शोषण एवं उत्पीड़नजन्य शीत से काँपती हुई मानवता को ठिठुरती धूप जैसी शिक्षा, संस्कृति व राजनीति कभी उष्णता प्रदान नहीं कर सकती। यह सब तभी, और मात्र तभी संभव है, जब वे स्वतः स्वस्थ हों, उनके रक्त में प्राणों की ऊष्मा हो। उन्हें स्वस्थ तथा सप्राण चित्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका चित्रण स्वस्थ चित्त से पूर्णतः तटस्थ तथा निष्पक्ष होकर किया जाए।
प्रस्तुत उपन्यास ‘ठिठुरती धूप’ में यही प्रयास किया गया है। अपने इस प्रयास में कथाकार को कितनी और क्या सफलता प्राप्त हुई है; उसका कथ्य, शिल्प तथा संप्रेष्य कितना सहज, सरस व प्रभविष्णु बन पड़ा है; यह सब तो पाठकों के विचार का विषय है। अतः उसके संबंध में यहाँ कुछ लिखना न तो उचित होगा और न न्यायसंगत ही, परंतु यहाँ यह लिखना अनुचित व असंगत न होगा कि इस उपन्यास का सृजन करते समय लेखकीय तटस्थ तथा निष्पक्षता बनाए रखने का भरसक प्रयास किया गया है। केवल संवाद लेखन के स्तर पर ही नहीं, प्रत्युत घटना-संयोजन, चरित्र-चित्रण तथा आत्मचिंतन के स्तर पर भी इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का प्रयास किया गया है।
यह भी निवेदन है कि उपन्यास के कथानक में वर्णित स्थान, पात्र, दल, संगठन, घटनाक्रम सब काल्पनिक हैं। किसी को लांछित करने के अभिप्राय से कुछ भी नहीं लिखा गया है। बस, प्रसंगवश देश में हुए राजनीतिक परिवर्तन एवं तत्कालीन केंद्र सरकार एवं कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख है, किंतु संबंधित विवरण कल्पना के नहीं, निकट अतीत के प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित हैं।
‘रिसता घाव’ उपन्यास के लेखन, प्रकाशन एवं विमोचन के पश्चात इस नवीन उपन्यास के लेखन, मुद्रण व प्रकाशन के प्रति मेरे पुत्रों—देवेंद्र, राजेंद्र, शैलेंद्र व सुधींद्र—की ही नहीं, मित्रों व शुभचिंतकों की जो उत्सुकता व आतुरता रही, उसके कारण इस उपन्यास के सृजन में तो कोई शैथिल्य एवं प्रमाद नहीं आया; परंतु कारणवश इस उपन्यास का प्रकाशन अवश्य विलंबित होता रहा।
अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस उपन्यास के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया कुछ भी क्यों न हो, परंतु इसे पढ़कर उन्होंने अपना श्रम व बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं किया, ऐसी अनुभूति उन्हें अवश्य होगी। इसी विश्वास के साथ मैं इस उपन्यास को सहर्ष सुधीजनों के करकमलों में सौंप रहा हूँ।
प्रतीक,
कनकनयाना
—रामनाथ नीखरा
पिछोर (शिवपुरी)
पिछोर (शिवपुरी)
:१:
रात का सन्नाटा अभी गहराया नहीं था। एकाकी अथवा अपने मित्र या संबंधी के
साथ कुछ लोग इधर से उधर तथा उधर से इधर आ-जा रहे थे। जब-तब टैंपो, टैक्सी,
मोटर साइकल, स्कूटर व कार की घरघराहट हॉस्पिटल के आसपास के विस्तृत
वातावरण में थरथराहट उत्पन्न कर देती थी। सुन कर उन्निद्र तारे जैसे पलकों
को झपकाकर चौकन्ने होने का अभिनय सा करने लगते थे, और पेड़ों पर बैठे
पक्षियों के झुंड़ अपने पर फड़फड़ाकर जाग्रत होने का आभास करा देते थे।
प्रशांत गहन चिकित्सा इकाई के कक्ष नंबर सात में रोगिणी के पार्श्व में
पड़ी कुरसी पर बैठकर उसकी नाड़ी देख रहा था। अकस्मात् रोगिणी के चेहरे पर
पड़ी हुई चादर का छोर हवा से उड़ा और उसका मुख पूर्णतः अनावृत हो गया।
नाड़ी देखते-देखते प्रशांत की दृष्टि सहसा उस पर जा पड़ी और मुँह से निकल
गया, ‘‘प्रमिला!....अरे यह तो प्रमिला
है।’’
डॉ. प्रशान्त पुरोहित विस्मय-विस्फारित नेत्रों को मौत से जूझती हुई रूग्णा के चेहरे पर टिकाए उसे अपलक दृष्टि से देखने लगा, मानो यह विश्वास कर लेना चाहता हो कि ढलती हुई रात्रि में विद्युत के मद्धिम प्रकाश में जिस रोगिणी को देखकर उसने यह निष्कर्ष निकाला है वह भ्रम नहीं, सत्य है; एक कठोर वास्तविकता है।
किंतु प्रमिला यहाँ क्यों आने लगी ?....यदि वह यहीं रहती है तो भी क्या वह आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगी ?.... नहीं-नहीं, प्रमिला जैसी विदुषी, बुद्धिमती स्त्री ऐसा कभी नहीं कर सकती....कदापि नहीं कर सकती....तो फिर यह कौन है ? आकृति तो ठीक प्रमिला जैसी ही है। प्रशांत का मन अपने-आप से ही संघर्ष कर रहा था....सद्यप्रफुल्लित पाटल पुष्प के सदृश अपने चारों ओर मुस्कान माधुरी बिखराती प्रमिला की मोहक मुखाकृति से इस म्लान, श्रीहीन चेहरे की भला क्या तुलना ? प्रशांत मानो अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर पूर्व निष्कर्ष को बदल देना चाहता था। उसने अपने आप से तर्क किया और सोचने लगा।
कोई तीन घंटे पूर्व, डॉ. मल्होत्रा के निर्देश पर जब वह इस गहन चिकित्सा इकाई में आया था, तब तो ऐसा कोई आभास उसे नहीं हुआ था। फिर इस अल्पावधि में ही ऐसा क्या हो गया कि यह रूग्णा उसे प्रमिला जैसी दिखाई पड़ने लगी ? नहीं, नहीं, उसे धोखा हुआ है।
धोखा ?....कैसा धोखा ? डॉ. मल्होत्रा ने उसे बुलाकर कहा था कि एक स्त्री ने अपनी पारिवारिक कठिनाइयों से घबड़ाकर प्राण देने का निर्णय लिया तथा नींद की कई गोलियाँ एक साथ खा लीं, और अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जाओ, उसे बचाने का यत्न करो। उनके इसी निर्देश पर वह इस गहन चिकित्सा इकाई में आया था और रात भर जागकर उसे बचाने का प्रयास करता रहा था। उस समय तो उसे यह नहीं लगा था कि यह रोगिणी प्रमिला है, लेकिन अब....? अब लगता है कि यह रोगिणी कोई और नहीं, प्रमिला है।....हूँ, तो कल या आज धोखा तो हुआ ही !
स्टेथस्कोप उठाकर वह अपने पलंग की ओर बढ़ा किंतु उसे लगा, जैसे कोई उसे पीछे धकेल रहा हो। धीरे-धीरे चलकर वह पलंग पर आ लेटा। उसकी आँखों के आगे कई वर्ष पुरानी यादों का काफिला आ धमका।
अपने गृहनगर में प्रशांत जिस मोहल्ले में रहता था, उसी में प्रमिला भी दो-एक मकान के अंतर पर रहती थी। यही नहीं, वह भी उसी हाई स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें प्रशांत पढ़ता था। अतः कभी-कभी पुस्तक के बहाने या अभ्यास पुस्तिका के बहाने वह उसके घर आया करती थी। उसके संयत तथा शालीन व्यवहार को देखकर प्रशांत की माँ ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं की थी...आपत्ति की कोई बात भी नहीं थी, प्रमिला पाठ्य-विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करती थी। उसकी स्वर्णलता सी देह में ऐसी कांति व कमनीयता थी जो उसे किसी के लिए भी चिरकाम्य बना सकती थी—बनाती भी थी। परंतु, न जाने क्यों, वह इस सबसे पूर्णतःअनभिज्ञ जैसी थी। और खुद प्रशांत ? वह प्रमिला के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं, उसके प्रति अनुरक्त भी था, परंतु उसने अपने इस भाव को कभी प्रमिला पर प्रकट नहीं होने दिया।
दिन, मास और वर्ष व्यतीत होते रहे। प्रमिला तथा उसने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और फिर इंटरमीडिएट में पढने लगे। संयोगवश यहाँ भी वे दोनों एक ही कक्षा के एक ही उपविभाग में पढ़ते थे। यही नहीं, प्रायः प्रायोगिक कार्य भी एक साथ करते थे।
‘‘सर, आपने यह तो बताया ही नहीं कि ओषधि कितने-कितने अंतराल से देनी है?’’ अकस्मात् डॉ. प्रशांत के सामने आकर कुमारी सरला मोघे ने पूछा।
‘‘एक इंजेक्शन तो अभी लगा दीजिए; शेष चार-चार घंटे के अंतराल से देती रहिए।’’ धीरे-गंभीर स्वर में प्रशांत ने उत्तर दिया।
‘‘जी, अच्छा।’’ कहकर नर्स पुनः गहन चिकित्सा इकाई में चली गई। उसके जाते ही प्रशांत का चिंतन पूर्ववत् प्रवाहित हो उठा।
इंटरमीडिएट के पश्चात उसे तो मेडिकल कोर्स के लिए चुन लिया गया और प्रमिला ने बी.एस-सी. में प्रवेश ले लिया। उसके पिता यद्यपि उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इंटरमीडिएट परीक्षा की योग्यता-सूची में स्थान पाने के कारण प्रमिला को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, इसी कारण उसने अपने अध्ययन में व्यतिक्रम नहीं आने दिया।
बी.एस-सी. करके उसने भौतिक विज्ञान विषय लेकर एम.एस-सी. में भी प्रवेश ले लिया।
‘कुहू, कुहू।’ हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर स्थित अमराई में कोयल कुहुक उठी। रात के उस सन्नाटे में उसे इस प्रकार कुहुकते सुनकर प्रशांत को लगा, जैसे वह कह रही हो, ‘रूको नहीं, कहो, फिर क्या हुआ ?’
‘हूँ।’ कहकर प्रशांत घटनाओं की संघटना पर विचार कर ही रहा था कि याद आया—जब वह एम.बी.बी.एस के चतुर्थ वर्ष में था, तब अवकाश लेकर घर आया हुआ था। एक दिन वह बैठा था कि प्रमिला आ गई। उसे देखकर लगा कि वह खूब रोकर आई है। ‘‘क्या बात है, प्रमिला ? तुमने रो-रोकर आँखे क्यों सुजा ली हैं ?’’ अवसर पाते ही प्रशांत ने पूछा था।
सुनते ही उसके आँसुओं का बांध टूट गया। रोती हुई बोली, ‘‘पिता जी विवाह करने पर तुले हुए हैं। परंतु मैं अभी करना नहीं चाहती।’’
‘‘बस यही बात है ? और कुछ तो नहीं ! वर तो तुम्हें पसंद है न ?’’ हठात् प्रशांत ने कुरेदा था।
‘‘यदि पसंद होता, तो मैं आपसे सहयोग माँगने क्यों आती ?’’ आँखों में आँखे डाल कर प्रमिला बोली, ‘‘फिर मेरी पसंद कौन है, क्या यह भी मुझे ही बताना होगा ? आपका हृदय क्या कहता है ? उसी से पूछो न!’’
सुनकर प्रशांत सकपका गया था। प्रमिला के हृदय में उसके लिए इतना आदर भाव है यह सोचकर प्रसन्नता हुई थी, परंतु साहस बटोर कर यह नहीं कह सका था कि ‘तुम्हारी इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ, प्रमिला, और यदि तुम्हारे पिता सहमत न हुए तो उनका विरोध करके भी मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तत्पर हूँ।’ इसके विपरीत, प्रमिला की बात सुनकर वह विचित्र ऊहापोह में पड़ गया था। और अंत में कहा था, ‘‘ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात करूँगा। उन्हें समझाने का प्रयत्न करूँगा।’’
‘‘ठीक है,’’ कहने को तो प्रमिला कह गई थी, परंतु उसके बुझे-बुझे चेहरे से लगता था कि उसे वह सब अच्छा नहीं लगा था। अतः वह वहाँ रुके बिना तत्काल चली गई थी और फिर..
‘‘डॉक्टर साहब, लगता है, आत्महत्या का प्रयास करने वाली रोगिणी को धीरे-धीरे होश आ रहा है।’’ कुमारी सरला मोघे ने प्रशांत के कमरे में पुनः प्रविष्ट होकर कहा।
‘‘ऐसा...? तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।’’ अपने चिंतन को विराम देकर प्रशांत ने कहा, ‘‘चलो, मैं भी चलता हूँ।’’
प्रशांत सरला के साथ गहन चिकित्सा इकाई में आ गया। वह सीधा पलंग के पास पहुँचा और उसके पार्श्व में पड़ी कुरसी पर बैठ प्रमिला की गतिविधियों को देखने लगा।
कुछ देर बाद प्रमिला ने नर्स की ओर मुड़कर पूछा, ‘‘मैं कहाँ हूँ ?’’
‘‘हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में।’’ प्रश्न यद्यपि नर्स से किया गया था, परंतु उत्तर डॉ. प्रशांत ने दिया।
डॉ. प्रशान्त पुरोहित विस्मय-विस्फारित नेत्रों को मौत से जूझती हुई रूग्णा के चेहरे पर टिकाए उसे अपलक दृष्टि से देखने लगा, मानो यह विश्वास कर लेना चाहता हो कि ढलती हुई रात्रि में विद्युत के मद्धिम प्रकाश में जिस रोगिणी को देखकर उसने यह निष्कर्ष निकाला है वह भ्रम नहीं, सत्य है; एक कठोर वास्तविकता है।
किंतु प्रमिला यहाँ क्यों आने लगी ?....यदि वह यहीं रहती है तो भी क्या वह आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगी ?.... नहीं-नहीं, प्रमिला जैसी विदुषी, बुद्धिमती स्त्री ऐसा कभी नहीं कर सकती....कदापि नहीं कर सकती....तो फिर यह कौन है ? आकृति तो ठीक प्रमिला जैसी ही है। प्रशांत का मन अपने-आप से ही संघर्ष कर रहा था....सद्यप्रफुल्लित पाटल पुष्प के सदृश अपने चारों ओर मुस्कान माधुरी बिखराती प्रमिला की मोहक मुखाकृति से इस म्लान, श्रीहीन चेहरे की भला क्या तुलना ? प्रशांत मानो अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर पूर्व निष्कर्ष को बदल देना चाहता था। उसने अपने आप से तर्क किया और सोचने लगा।
कोई तीन घंटे पूर्व, डॉ. मल्होत्रा के निर्देश पर जब वह इस गहन चिकित्सा इकाई में आया था, तब तो ऐसा कोई आभास उसे नहीं हुआ था। फिर इस अल्पावधि में ही ऐसा क्या हो गया कि यह रूग्णा उसे प्रमिला जैसी दिखाई पड़ने लगी ? नहीं, नहीं, उसे धोखा हुआ है।
धोखा ?....कैसा धोखा ? डॉ. मल्होत्रा ने उसे बुलाकर कहा था कि एक स्त्री ने अपनी पारिवारिक कठिनाइयों से घबड़ाकर प्राण देने का निर्णय लिया तथा नींद की कई गोलियाँ एक साथ खा लीं, और अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जाओ, उसे बचाने का यत्न करो। उनके इसी निर्देश पर वह इस गहन चिकित्सा इकाई में आया था और रात भर जागकर उसे बचाने का प्रयास करता रहा था। उस समय तो उसे यह नहीं लगा था कि यह रोगिणी प्रमिला है, लेकिन अब....? अब लगता है कि यह रोगिणी कोई और नहीं, प्रमिला है।....हूँ, तो कल या आज धोखा तो हुआ ही !
स्टेथस्कोप उठाकर वह अपने पलंग की ओर बढ़ा किंतु उसे लगा, जैसे कोई उसे पीछे धकेल रहा हो। धीरे-धीरे चलकर वह पलंग पर आ लेटा। उसकी आँखों के आगे कई वर्ष पुरानी यादों का काफिला आ धमका।
अपने गृहनगर में प्रशांत जिस मोहल्ले में रहता था, उसी में प्रमिला भी दो-एक मकान के अंतर पर रहती थी। यही नहीं, वह भी उसी हाई स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें प्रशांत पढ़ता था। अतः कभी-कभी पुस्तक के बहाने या अभ्यास पुस्तिका के बहाने वह उसके घर आया करती थी। उसके संयत तथा शालीन व्यवहार को देखकर प्रशांत की माँ ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं की थी...आपत्ति की कोई बात भी नहीं थी, प्रमिला पाठ्य-विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करती थी। उसकी स्वर्णलता सी देह में ऐसी कांति व कमनीयता थी जो उसे किसी के लिए भी चिरकाम्य बना सकती थी—बनाती भी थी। परंतु, न जाने क्यों, वह इस सबसे पूर्णतःअनभिज्ञ जैसी थी। और खुद प्रशांत ? वह प्रमिला के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं, उसके प्रति अनुरक्त भी था, परंतु उसने अपने इस भाव को कभी प्रमिला पर प्रकट नहीं होने दिया।
दिन, मास और वर्ष व्यतीत होते रहे। प्रमिला तथा उसने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और फिर इंटरमीडिएट में पढने लगे। संयोगवश यहाँ भी वे दोनों एक ही कक्षा के एक ही उपविभाग में पढ़ते थे। यही नहीं, प्रायः प्रायोगिक कार्य भी एक साथ करते थे।
‘‘सर, आपने यह तो बताया ही नहीं कि ओषधि कितने-कितने अंतराल से देनी है?’’ अकस्मात् डॉ. प्रशांत के सामने आकर कुमारी सरला मोघे ने पूछा।
‘‘एक इंजेक्शन तो अभी लगा दीजिए; शेष चार-चार घंटे के अंतराल से देती रहिए।’’ धीरे-गंभीर स्वर में प्रशांत ने उत्तर दिया।
‘‘जी, अच्छा।’’ कहकर नर्स पुनः गहन चिकित्सा इकाई में चली गई। उसके जाते ही प्रशांत का चिंतन पूर्ववत् प्रवाहित हो उठा।
इंटरमीडिएट के पश्चात उसे तो मेडिकल कोर्स के लिए चुन लिया गया और प्रमिला ने बी.एस-सी. में प्रवेश ले लिया। उसके पिता यद्यपि उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इंटरमीडिएट परीक्षा की योग्यता-सूची में स्थान पाने के कारण प्रमिला को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, इसी कारण उसने अपने अध्ययन में व्यतिक्रम नहीं आने दिया।
बी.एस-सी. करके उसने भौतिक विज्ञान विषय लेकर एम.एस-सी. में भी प्रवेश ले लिया।
‘कुहू, कुहू।’ हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर स्थित अमराई में कोयल कुहुक उठी। रात के उस सन्नाटे में उसे इस प्रकार कुहुकते सुनकर प्रशांत को लगा, जैसे वह कह रही हो, ‘रूको नहीं, कहो, फिर क्या हुआ ?’
‘हूँ।’ कहकर प्रशांत घटनाओं की संघटना पर विचार कर ही रहा था कि याद आया—जब वह एम.बी.बी.एस के चतुर्थ वर्ष में था, तब अवकाश लेकर घर आया हुआ था। एक दिन वह बैठा था कि प्रमिला आ गई। उसे देखकर लगा कि वह खूब रोकर आई है। ‘‘क्या बात है, प्रमिला ? तुमने रो-रोकर आँखे क्यों सुजा ली हैं ?’’ अवसर पाते ही प्रशांत ने पूछा था।
सुनते ही उसके आँसुओं का बांध टूट गया। रोती हुई बोली, ‘‘पिता जी विवाह करने पर तुले हुए हैं। परंतु मैं अभी करना नहीं चाहती।’’
‘‘बस यही बात है ? और कुछ तो नहीं ! वर तो तुम्हें पसंद है न ?’’ हठात् प्रशांत ने कुरेदा था।
‘‘यदि पसंद होता, तो मैं आपसे सहयोग माँगने क्यों आती ?’’ आँखों में आँखे डाल कर प्रमिला बोली, ‘‘फिर मेरी पसंद कौन है, क्या यह भी मुझे ही बताना होगा ? आपका हृदय क्या कहता है ? उसी से पूछो न!’’
सुनकर प्रशांत सकपका गया था। प्रमिला के हृदय में उसके लिए इतना आदर भाव है यह सोचकर प्रसन्नता हुई थी, परंतु साहस बटोर कर यह नहीं कह सका था कि ‘तुम्हारी इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ, प्रमिला, और यदि तुम्हारे पिता सहमत न हुए तो उनका विरोध करके भी मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तत्पर हूँ।’ इसके विपरीत, प्रमिला की बात सुनकर वह विचित्र ऊहापोह में पड़ गया था। और अंत में कहा था, ‘‘ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात करूँगा। उन्हें समझाने का प्रयत्न करूँगा।’’
‘‘ठीक है,’’ कहने को तो प्रमिला कह गई थी, परंतु उसके बुझे-बुझे चेहरे से लगता था कि उसे वह सब अच्छा नहीं लगा था। अतः वह वहाँ रुके बिना तत्काल चली गई थी और फिर..
‘‘डॉक्टर साहब, लगता है, आत्महत्या का प्रयास करने वाली रोगिणी को धीरे-धीरे होश आ रहा है।’’ कुमारी सरला मोघे ने प्रशांत के कमरे में पुनः प्रविष्ट होकर कहा।
‘‘ऐसा...? तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।’’ अपने चिंतन को विराम देकर प्रशांत ने कहा, ‘‘चलो, मैं भी चलता हूँ।’’
प्रशांत सरला के साथ गहन चिकित्सा इकाई में आ गया। वह सीधा पलंग के पास पहुँचा और उसके पार्श्व में पड़ी कुरसी पर बैठ प्रमिला की गतिविधियों को देखने लगा।
कुछ देर बाद प्रमिला ने नर्स की ओर मुड़कर पूछा, ‘‘मैं कहाँ हूँ ?’’
‘‘हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में।’’ प्रश्न यद्यपि नर्स से किया गया था, परंतु उत्तर डॉ. प्रशांत ने दिया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book